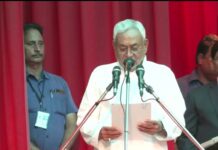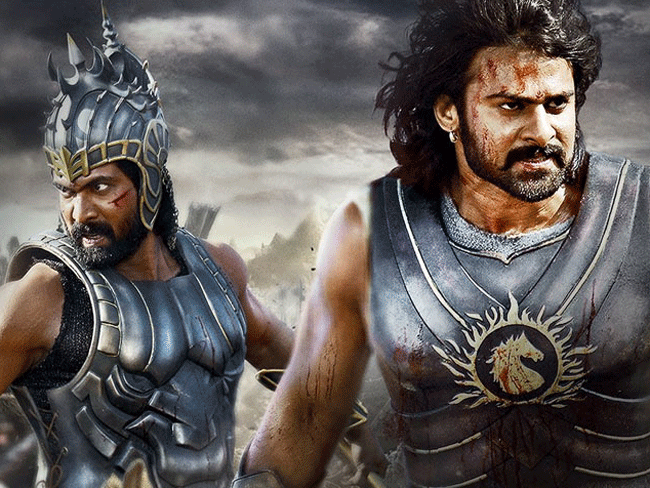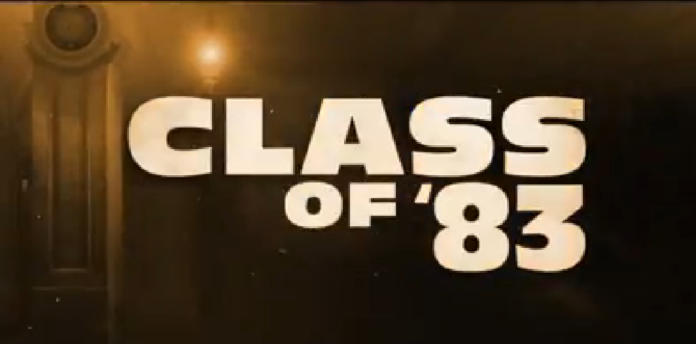क्लास ऑफ ’83 पूरे एक घण्टे 38 मिनट तनाव बनाकर रखती है, जो इस जेनर की फिल्म के लिए एक आवश्यक तत्व है। पर उसका असर बस फ़िल्म तक ही रहता है. आपको गॉडफादर का वो दृश्य याद होगा जिसमें गॉडफादर के बेटे का करदार निभा रहे अलपचीनो एक रेस्तरां में अपने बाप के दुश्मनों को गोली मारते हैं। उस दृश्य में और खासकर अलपचीनो के चेहरे पर इतना तनाव है कि एक लम्हे के लिए लगता है स्क्रीन फट जाएगी। क्लास ऑफ 83 में कई तनाव के क्षण हैं। वो दृश्य जिसमें सब इंस्पेक्टर शुक्ला एक गैंगस्टर के ठीक सामने बैठे हैं. एक दूसरे दृश्य जिसमें सब इंस्पेक्टर असलम बदमाशों के बीच फंस गए हैं। अगर लेखक, अभिनेता और निर्देशक मिलकर दृश्यों को और टेन्स कर सकते तो बेहतर होता। क्लाइमैक्स बहुत रूटीन बल्कि बचकाने ढंग से फिल्माया गया है। जिस कलसेकर को पहली बार मंत्री बचा लेता है, वही उसे दूसरी बार बचाने नहीं आता। लगता है तब तक डाइरेक्टर थक गए थे और समझ गए थे की फिल्म के लिए उन्होने गलत कहानी चुन ली है।

फिल्म ट्रेनिंग स्कूल तक तो ठीक चलती है, फिर भी वो कल्ट क्लैसिक प्रहार की बराबरी नहीं कर पाती, शायद इसलिए कि निर्देशक (और लेखक) के रूप में नाना पाटेकर को फिल्म की ट्रेजक्टरी पता थी, शायद इसलिए कि यहाँ इंस्ट्रक्टर या डीन के रूप में नाना पाटेकर जैसा अभिनेता नहीं है, शायद इसलिए कि वो हॉस्टल लाइफ में क्लीशे का कुछ ज़्यादा ही सहारा ले लेती है, और आप बेचैनी से सोचते हैं – नहीं, ये इस फ़िल्म की थीम नहीं है, प्लीज इसे मत दिखाओ, ये मख़मल में टाट के पैबंद जैसा है, ये फ़ैमिली आडियन्स को दूर कर देगा। यहाँ निर्देशक बहुत निराश करते हैं।
फ़िल्म का सम्पादन बहुत अच्छा है। फ़िल्म की लम्बाई बढ़ानी मुश्किल थी क्यूंकि ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं।
फ़िल्म में कहीं भी पुलिसवालों को बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहने नहीं दिखाया गया है। इसी चूक की वजह से 6 पुलिसवाले कलसेकर के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं। फ़िल्म बॉबी देओल द्वारा 5 कैडेट्स को चुनने की जो वजह बताती है वो कन्विंसिंग नहीं है। कहानी आज के हिसाब से मौजू नहीं है. आज के समय में 1983 में पुलिस के इस तरह एंकाउंटर करने से आप खुद को रिलेट नहीं कर पाते। हम बहुत आगे आ गए हैं, हमारा वक़्त दूसरा है, इसकी मुसीबतें और बारीकियाँ अलग हैं।

निर्देशक अतुल सभरवाल ने 2010 सोनी टीवी और यशराज फिल्म्स के लिए “पाउडर” धारावाहिक बनाया था, जो मुंबई में ड्रग्स के धंधे को लेकर था। उसके संवाद उसे ऊपर उठाते थे। एक दृश्य में नोरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफ़सर मुंबई पुलिस से एक अपराधी वसीम की कस्टडी लेने गए हैं। पुलिस के ये पूछने पर कि “और 407 फाइलें हैं एनसीबी में, लेकिन उनमें से ख़ास वसीम की कस्टडी के लिए आप लोग यहाँ आए हैं,” वो जवाब देते हैं – “हाँ, हमने 407 नामों की पर्ची डाली, जब एक निकाली तो वसीम के नाम की निकली।” इस तरह के इंटेलिजेंट डाइलॉग “क्लास ऑफ 83” में मिसिंग हैं। निर्देशक प्रतिभावान हैं। उसकी झलक कुछ दृश्यों में मिलती है. एक दृश्य में क्लास में खड़े शुक्ला को उसके पास का कैडेट बैठने के लिए बोलता है। दूसरे दृश्य में जब सब इंस्पेक्टर शुक्ला एक अख़बार के दफ़्तर में संपादक का कालर पकड़े है और उसकी बीवी दूसरी तरफ़ मुंह कर लेती है।
इन दिनों लेखक किरदारों को उभारने में मदद नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि बहुत से किरदार एक ही जैसे सोचते बोलते हैं और वे अलग से याद नहीं रह जाते। उनका अपना कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। वो एक समूह बन जाते हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है। जबकि हर चरित्र का अपना एक रंग होना चाहिए।
1957 एक एक फ़िल्म “दीदार” के एक दृश्य में अशोक कुमार, गरीब और अंधे दिलीप कुमार की आँखों की जांच कर रहे हैं। बाहर फर्श पर निम्मी और उनका एक दोस्त बैठा है।
निम्मी कहती हैं – “आस न तोड़ना भगवन, आस न तोड़ना।”
दोस्त – “…ये आँखों की चीरफाड़ में कहीं दम तो नहीं तोड़ दिया भइया ने।”
निम्मी – “ऐसी मनहूस बातें न किया कर बल्लम, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे भी जान से मार डालूँगी।”
दोस्त – “…जान से मारने की क्या ज़रूरत है पगली। अगर भइया लंबे हो गए तो हम खुद ही सूख-सूख कर मर जाएंगे।”

इस सीन में चार चरित्र हैं। सब का अपना अलग-अलग व्यक्तित्व है। दोस्त दिलीप कुमार का बचपन का साथी है, पर यहाँ भी वो मज़ाक करना नहीं छोड़ता। “क्लास ऑफ 83” में पाँचों कडेट्स की इंडिविजुअलिटी उभर कर सामने नहीं आती। ये हमारे ज़माने के सिनेमा का दोष है। वो चरित्रों पर मेहनत नहीं करता। क्या आपको ऐसे चरित्र याद हैं जो थोड़ी देर के लिए आए और आप सोचने लगे वो कौन था. “प्यासा” में सम्पादक का वो असिस्टेंट, “स्पाइडर मैन” में जर्मन मकान मालिक की लड़की, “अपूर संसार” में नायक का हमनाम पड़ोसी।
सब इंस्पेक्टर शुक्ला का किरदार निभा रहे भूपेंद्र जादावत ने एनएसडी की अपनी ट्रेनिंग की वजह से अपने किरदार को बहुत अच्छे ढंग से कैरी किया है। उन्हें इस फ़िल्म के बाद भी देखने का इंतज़ार रहेगा.
फ़िल्म कहती है कि वो मोटे तौर पर सय्यद हुसैन जैदी की 2019 में आई किताब “द पनिशर्स ऑफ मुंबई पुलिस, द क्लास ऑफ 83” पर आधारित है। उनकी कई किताबों पर फिल्में बनी हैं। 1993 के दंगों पर आधारित “ब्लैक फ्राइडे” पर अनुराग कश्यप ने इसी नाम से फ़िल्म बनाई थी, जो बैन हुयी और अब जाकर प्राइम पर आ पाई है।
बैक्ग्राउण्ड स्कोर विजू शाह का है। निर्देशक वही 80 के दशक का सिंथ म्यूजिक चाहते थे इसलिए। 80 के दशक की बंबई का प्रभाव लाने के लिए निर्देशक ने फ़िल्म डिविजन की डाक विभाग, नेशनल पुलिस अकादमी आदि पर बनी डॉक्युमेंट्रीज़ को खंगाला और उस समय को रिक्रिएट करने की कोशिश की। उन्होने पुरानी फ़िल्मों के दृश्य भी डाले।
फ़िल्म का क्लाइमैक्स अनकन्विंसिंग है। कहानी कंटेम्पररी नहीं है, इंगेज करने वाली भी नहीं है। जो है, उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं है। किरदारों पर मेहनत नहीं की गयी है। बस एक किताब है, जिस पर एक फ़िल्म बनी है। अब किताब कैसी है, वो एक अलग लेख का विषय है.