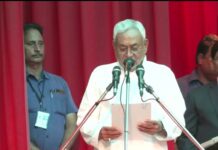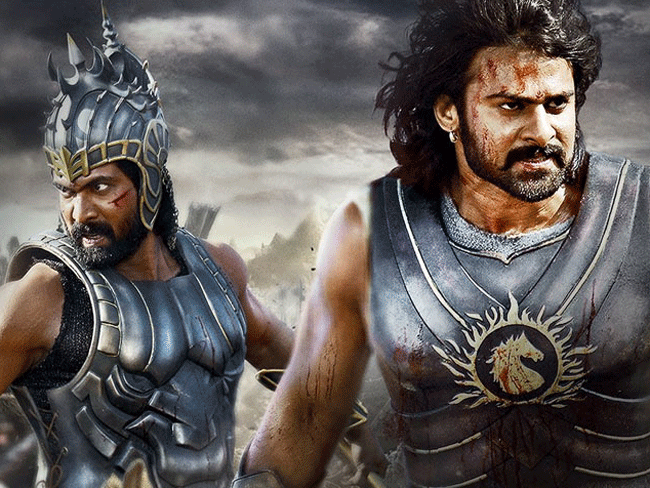अंसारी मंसूरी कुरैशी राईन सैफी और भी बहुत सी जातियां, जो कुल मुसलमानों का 85% हैं वो दलित हैं पिछड़ा है पसमांदा हैं और भारत के मूल निवासी हैं। पसमांदा,जो कि एक फारसी शब्द है, का अर्थ होता है। ‘वह जो पीछे छूट गया’। बिहार में 1998 में अली अनवर के नेतृत्व में ‘ऑल इण्डिया पसमांदा मुस्लिम महाज़’ के गठन और उनकी लिखी किताब ‘मसावात की जंग (2001)’ के चलते यह शब्द काफी लोकप्रिय हुआ। इसके पहले डॉ. एजाज़ अली के नेतृत्व में ‘ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा’ दलित मुसलमान शब्द चर्चा में ला चुका था. अली अनवर की किताब ने बिहार के पसमांदा मुसलमानों की दयनीय स्थिति के बारे में ज़ोरदार बहस को पैदा किया और पसमांदा राजनीति की ज़मीन तैयार की। बेशक मुस्लिम समाज में कमज़ोर जातियों के आंदोलनों का इतिहास पुराना है। आजादी के पहले से ऑल इण्डिया मोमिन कान्फ्रेंस का हस्तक्षेप, खास तौर पर जिन्ना के दो राष्ट्रों के नज़रिए और बंटवारे का सीधा विरोध, काबिलेतारीफ है। मगर डॉ. एजाज़ अली और अली अनवर के हस्तक्षेप के बाद पसमांदा विमर्श ने एक गुणात्मक छलांग लगाई है, इस पर दो मत नहीं हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड जैसे प्रदेशों में कई पसमांदा संगठन खड़े हो रहे हैं और संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं।
मुसलमानों में तीन वर्ण

अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंतो अअशराफ़ 15% और पिछड़े (अजलाफ़) और दलित (अरजाल) मुसलमान भारतीय मुसलमानों की कुल आबादी का कम-से-कम 85 फीसद होते हैं। पसमांदा आंदोलन, बहुजन आंदोलन की तरह, मुसलमानों के पिछड़े और दलित तबकों की नुमाइंदगी करता है और उनके मुद्दों को उठाता है। यह भारत के मुसलमानों की अकलियती सियासत को अशराफिया राजनीति मानता है और उसे चुनौती देता है।
आखिर क्या है अशराफिया राजनीति?

यह मुसलमानों की अगड़ी जातियों की राजनीति है जो सिर्फ कुछ सांकेतिक और जज्बाती मुद्दों — जैसे बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ इत्यादि — को उठाती रही है। इन मुद्दों पर गोलबंदी करके और अपने पीछे मुसलमानों का हुजूम दिखा के मुसलमानों की अगड़ी बिरादरियां और उनके दबदबे में चलने वाले संगठन (जमीअत-ए-उलेमा-ए-हिन्द, जमात-ए-इस्लामी, आल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरात, पॉपुलर फ्रण्ट ऑफ इण्डिया इत्यादि) अपना हित साधते रह कर सत्ता में अपनी जगह पक्की करते रहे हैं। इनका पूरा तर्ज़े-अमल गैर-जम्हूरी है. ये इस तरह के जज्बाती मुद्दों के ज़रिये अपना प्रतिनिधित्व तो कर लेते हैं मगर पसमांदा मुसलमानों की बलि चढ़ जाती है. बजाहिर यह पसमांदा तबके के कुछ व्यक्तियों को, जिनका ‘अशराफिकरण’ हो चुका है और जो अगड़े मुसलमानों की तहज़ीबी गुलामी करते हैं और उस पर फख्र करते हैं, को आगे तो रखते हैं लेकिन किसी नेकनियती से नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के अंदरूनी जातपात के तजाद को काबू में रखने के लिए. दिलचस्प बात है कि इन्हीं मुद्दों—बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ पर इनकी राजनीति फलती-फूलती है।
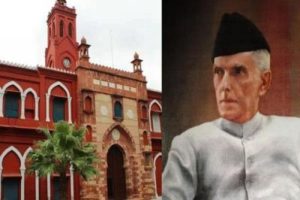
ज़ाहिर है कि इस जज़्बाती राजनीति में पसमांदा आबादी, जिनमें ज़्यादातर कारीगर-दस्तकार हैं और मेहनत-मजदूरी कर के अपना गुज़र बसर करते हैं, के मुद्दे और परेशानियों के लिए जगह कहाँ हो सकती है? मुख्यधारा की मुस्लिम संस्कृति में क़व्वाली, ग़ज़ल, दास्तानगोई, कुरान के ऊपर अक्ली कसरत का तो शुमार होगा लेकिन बक्खो के गीत, जुलाहों का करघा, मीरशिकार के किस्सों का ज़िक्र कैसे हो सकता है. मुस्लिम लीडरान और मशहूर हस्तियों में अशराफ़ तबके के अबुल कलाम आज़ाद, सर सैय्यद अहमद खान, मुहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल वगैरह का ज़िक्र तो होना ही है मगर पसमांदा तबके के अब्दुल कैयूम अंसारी, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अतीकुर्रहमान आरवी मंसूरी, आसिम बिहारी के लिए कोई गुंजाईश कहाँ?
मुस्लिम एकता का नारा घाटे का सौदा

इस बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि ‘मुस्लिम’ राजनीति से पसमांदा मुसलमानों का कोई लाभ नहीं होने वाला है. ‘मुस्लिम एकता’ का नारा पसमांदा मुसलमानों के लिए घाटे का सौदा है. ये राजनीतियां दोनों धर्मों की कमज़ोर जातियों को मज़हबी पागलपन में झोंक कर अगड़ी जातियों के मफाद को महफूज़ करने का काम करती हैं।

इस लिए धार्मिक पहचान के आधार पर एकता की जगह सभी धर्मों की कमज़ोर जातियों की एकता पर ध्यान देना होगा. ज़ाहिर सी बात है कि इस से ‘इस्लाम खतरे में है’ का नारा कमजोर होगा। देश की पसमांदा आबादी को अब समझ लेना चाहिए कि जिस ‘इस्लाम’ की ओर ये नारे इशारा कर रहे हैं वे उनके नहीं. उन के इस्लाम की कुछ नयी व्याख्याएं हुई हैं और काफी अभी होनी बाक़ी है. वक्त के साथ जब ये तबके कलम पकड़ेंगे तो वह भी मुमकिन होगा।